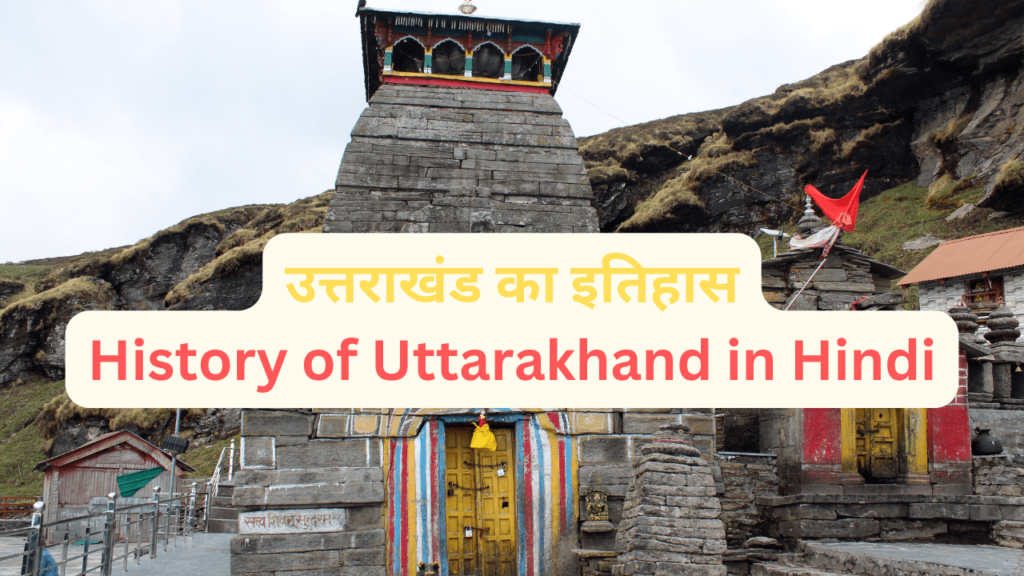
History of Uttarakhand in Hindi : उत्तराखण्ड, भारत के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है इसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश से अलग करके इसे 2000 में बनाया गया था और इसे “देवभूमि” या देवताओं का निवास भी कहा जाता है इस राज्य का इतिहास प्राचीन समय से ही बहुत खास रहा है। यहाँ ऋषि-मुनियों ने तपस्या की, और यह स्थान महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों से जुड़ा हुआ है। इस लेख में हम उत्तराखंड के इतिहास का अध्ययन करेंगे।
Index of History of Uttarakhand in Hindi
उत्तराखंड का इतिहास एक लंबी और समृद्ध यात्रा है, जिसे तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मानव सभ्यता के शुरुआती प्रमाण जैसे पाषाण युग के उपकरण और शैल चित्र मिलते हैं। दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल, जो प्राचीन लेखन और संस्कृतियों से जुड़ा है। तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल, जिसे प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल में बांटा गया है। प्राचीन काल में शुरुआती सभ्यताएँ और धार्मिक जीवन था, मध्य काल में विभिन्न राजवंशों का शासन था, और आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएँ शामिल हैं।
प्रागैतिहासिक काल (Prehistoric Period)
प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें पाषाणकालीन उपकरणों, गुफाओं, शैल चित्रों, कंकालों, और धातु उपकरणों के माध्यम से मिलती है। इस काल के प्रमुख साक्ष्य निम्नलिखित हैं:
- लाखु गुफा
- स्थितिः अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में।
- खोजः 1963 में।
- विशेषताः गुफा में मानव और पशुओं के चित्र मिले हैं, जिनमें मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इन चित्रों को रंगों से सजाया गया है।
- ग्वारख्या गुफा
- स्थितिः चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे डुग्री गाँव।
- विशेषताः यहाँ मानव, भेड़, लोमड़ी, और बारहसिंगा के रंगीन चित्र पाए गए हैं।
- मलारी गाँव
- स्थितिः चमोली जिले में।
- खोजः गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 2002 में।
- विशेषताः यहाँ से हजारों वर्ष पुराने नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन और 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है। मिट्टी के बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी की शैली से मिलते-जुलते हैं।
- किमनी गाँव
- स्थितिः चमोली जिले के थराली के पास।
- विशेषताः यहाँ हथियारों और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं।
- ल्वेथाप
- स्थितिः अल्मोड़ा।
- विशेषताः शैल चित्रों में मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है।
- बनकोट
- स्थितिः पिथौरागढ़।
- विशेषताः यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं।
- फलसीमा
- स्थितिः अल्मोड़ा जिला।
- विशेषताः यहाँ योग और नृत्य मुद्रा में मानव आकृतियाँ पाई गई हैं।
- हुडली
- स्थितिः उत्तरकाशी।
- विशेषताः नीले रंग से रंगे शैल चित्र यहाँ मिले हैं।
- पेटशाल
- स्थितिः अल्मोड़ा।
- विशेषताः यहाँ कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ पाई गई हैं।
इन साक्ष्यों से पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में उत्तराखंड में मानव जीवन और उसकी गतिविधियाँ न केवल विविध थीं, बल्कि कला और संस्कृति के प्रति उनकी गहरी रुचि भी थी।
आद्य ऐतिहासिक काल (Protohistoric Period)
आद्य ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है इस काल के बारे में जानकारी विभिन्न धार्मिक ग्रंथो से मिलती है | इस काल का विस्तार चतुर्थ शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना जाता है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जिसमे इसे देवभूमि एवं मनीषियों की पुण्य भूमि कहा गया है ऐतरेव ब्राहमण में इस क्षेत्र लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। विभिन्न ग्रंथों में गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिलती है।
गढ़वाल क्षेत्र
गढ़वाल क्षेत्र को पहले बद्रिकाश्रम, स्वर्गभूमि, तपोभूमि आदि नामों से जाना जाता था, लेकिन 1515 ई. में पवार शासक अजयपाल द्वारा 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा।
ऋग्वेद के अनुसार, यहाँ के प्राण गाँव में सप्त ऋषियों ने प्रलय के बाद अपने प्राणों की रक्षा की। इसके अलावा, अल्कापुरी (कुबेर की राजधानी) को आदि मनु का निवास स्थल माना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र के बदरीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी।
देवप्रयाग के सितोनस्यु पट्टी में सीता जी के पृथ्वी में समाने की कथा प्रसिद्ध है, जिसके कारण यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। रामायण काल में बाणासुर की राजधानी ज्योतिश्पुर (जोशीमठ) थी। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी।
इस क्षेत्र में प्राचीन काल में कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम जैसे विद्यापीठ थे। कण्वाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है, और यहाँ सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम “भारत” पड़ा। कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित था, और महाकवि कालिदास ने यहाँ “अभिज्ञान शकुंतलम” की रचना की थी। इस स्थान को आज चौकाघाट के नाम से जाना जाता है।
देहरादून के कालसी में अशोक के 257 ई. पू. के पाली भाषा में स्थापित अभिलेख मिले हैं, जिसमें पुलिंद और आपरांत शब्दों का प्रयोग हुआ है। देहरादून के लाखामंडल से राजकुमारी इश्वरा का शिलालेख भी मिला है।
कुमाऊँ क्षेत्र
कुमाऊँ का नाम चम्पावत के पास स्थित कान्तेश्वर पर्वत के नाम पर पड़ा। कुमाऊँ का सबसे अधिक उल्लेख स्कंदपुराण के मानसखंड में मिलता है। ब्रह्म और वायु पुराण के अनुसार, यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि जातियाँ निवास करती थीं। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है।
किरातों के वंशज अस्कोट और डोडीहाट नामक स्थानों में निवास करते हैं।
ऐतिहासिक काल (Historical Period)
उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल विभिन्न महाकाव्य, पौराणिक कथाओं और प्राचीन लेखों से जुड़ा हुआ है। इस काल को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्य काल, और आधुनिक काल।
प्राचीन काल ( Ancient Period )
प्राचीन कल में उत्तराखंड पर अनेक जातियों ने शासन किया जिनमे से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है
कुणिन्द शासक
- कुणिन्द उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनैतिक शक्ति थी |
- अशोक के कालसी अभिलेख से ज्ञात होता है की कुणिन्द प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे |
- कुणिन्द वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोधभूति था |
- अमोधभूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के मैदानी भागो पर शको ने अधिकार कर लिया , शको के बाद तराई वाले भागो में कुषाणों ने अधिकार कर लिया |
- उत्तराखंड में यौधेयो के शाशन के भी प्रमाण मिलते है इनकी मुद्राए जौनसार बाबर तथा लेंसडाउन ( पौड़ी ) से मिली है |
- ‘ बाडवाला यज्ञ वेदिका ‘ का निर्माण शीलवर्मन नामक राजा ने किया था , शील वर्मन को कुछ विद्वान कुणिन्द व कुछ यौधेय मानते है |
कर्तपुर राज्य
- कर्तपुर राज्य के संस्थापक भी कुणिन्द ही थे कर्तपुर में उत्तराखंड , हिमांचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग सामिल था |
- कर्तपुर के कुणिन्दो को पराजित कर नागो ने उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया |
- नागो के बाड़ कन्नोज के मौखरियो ने उत्तराखंड पर शासन किया |
- मौखरी वंश का अंतिम शासक गृह्वर्मा था हर्षवर्धन ने इसकी हत्या करके शासन को अपने हाथ में ले लिया |
- हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री व्हेनसांग उत्तराखंड भ्रमण पर आया था |
कार्तिकेयपुर राजवंश
- हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड पर अनेक छोटी – छोटी शक्यियो ने शासन किया , इसके पश्चात 700 ई . में कर्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुइ , इस वंश के तीन से अधिक परिवारों ने उत्तराखंड पर 700 ई . से 1030 ई. तक लगभग 300 साल तक शासन किया |
- इस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है |
- प्रारंभ में कर्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी जोशीमठ (चमोली ) के समीप कर्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी बाद में राजधानी बैजनाथ (बागेश्वर ) बनायीं गयी |
- इस वंस का प्रथम शासक बसंतदेव था बसंतदेव के बाद के राजाओ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलाती है इसके बाद खर्परदेव के शासन के बारे में जानकारी मिलती है खर्परदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था इसके बाद इसका पुत्र कल्याण राजा बना , खर्परदेव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था |
- नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेय राजवंश में खर्परदेव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई , निम्बर ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था
- निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना उसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था जागेश्वर में नवदुर्गा , महिषमर्दिनी , लकुलीश तथा नटराज मंदिरों का निर्माण कराया |
- इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित्शूर देव शासक बना तथा ललित्शूर देव के बाद उसका पुत्र भूदेव शासक बना इसने बौध धर्मं का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर निर्माण में सहयोग दिया |
- कर्तिकेयपुर राजवंश में सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की
- कर्तिकेयपुर शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आये उन्होंने बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया | सन 820 ई . में केदारनाथ में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया |
- कर्तिकेयपुर शासको की राजभाषा संस्कृत तथा लोकभाषा पाली थी |
मध्य काल (Medieval Period)
मध्यकाल के इतिहास में हम कत्यूरी शासन , चन्द वंश तथा गढ़वाल के परमार (पवांर ) वंश के बारे में अध्ययन करेंगे |
कत्यूरी वंश
- मध्यकाल में कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन था इसके बारे में जानकारी हमें स्थानीय लोकगाथाओं व जागर से मिलती है कर्तिकेयपुर वंश के बाद कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन हुआ |
- सन् 740 ई. से 1000 ई. तक गढ़वाल व कुमाऊं पर कत्यूरी वंश के तीन परिवारों का शासन रहा , तथा इनकी राजधानी कर्तिकेयपुर (जोशीमठ) थी|
- आसंतिदेव ने कत्यूरी राज्य में आसंतिदेव वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचुलाकोट में स्थापित की |
- कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था यह एक अत्याचारी शासक था जागरो में इसे वीरमदेव कहा गया है|
- जियारानी की लोकगाथा के अनुसार 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया और ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया और इसी आक्रमण के बाद कत्यूरी वंश का अंत हो गया|
- 1191 में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोकचल्ल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्ज़ा कर लिया|
- 1223 ई. में नेपाल के शासक काचल्देव ने कुमाऊॅ पर आक्रमण कर लिया और कत्यूरी शासन को अपने अधिकार में ले लिया।
कुमाऊं का चन्द वंश
- कुमाऊं में चन्द वंश का संस्थापक सोमचंद था जो 700 ई. में गद्दी पर बैठा था|
- कुमाऊं में चन्द और कत्यूरी प्रारम्भ में समकालीन थे और उनमें सत्ता के लिए संघर्ष चला जिसमें अन्त में चन्द विजयी रहे। चन्दों ने चम्पावत को अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभ में चम्पावत के आसपास के क्षेत्र ही इनके अधीन थे लेकिन बाड़ में वर्तमान का नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि क्षेत्र इनके अधीन हो गए|
- राज्य के विस्तृत हो जाने के कारण भीष्मचंद ने राजधानी चम्पावत से अल्मोड़ा स्थान्तरित कर दी जो कल्यांचंद तृतीय के समय (1560) में बनकर पूर्ण हुआ|
- इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़ चन्द था|
- कल्याण चन्द चतुर्थ के समय में कुमाऊं पर रोहिल्लो का आक्रमण हुआ| तथा प्रशिद्ध कवी ‘शिव’ ने कल्याण चंद्रौदयम की रचना की|
- चन्द शासन काल में ही कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमि निर्धारण की प्रथा प्रारंभ हुई|
- चन्द राजाओ का राज्य चिन्ह गाय थी|
- 1790 ई. में नेपाल के गोरखाओं ने चन्द राजा महेंद्र चन्द को हवालबाग के युद्ध में पराजित कर कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया , इसके सांथ ही कुमाऊं में चन्द राजवंश का अंत हो गया|
गढ़वाल का परमार (पंवार) राजवंश
- 9 वीं शताब्दी तक गढ़वाल में 54 छोटे-बड़े ठकुरी शासको का शासन था, इनमे सबसे शक्तिशाली चांदपुर गड का राजा भानुप्रताप था , 887 ई. में धार (गुजरात) का शासक कनकपाल तीर्थाटन पर आया, भानुप्रताप ने इसका स्वागत किया और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया।
- कनकपाल द्वारा 888 ई. में चाँदपुरगढ़ (चमोली) में परमार वंश की नींव रखीं, 888 ई. से 1949 ई. तक परमार वंश में कुल 60 राजा हुए।
- इस वंश के राजा प्रारंभ में कर्तिकेयपुर राजाओ के शामंत रहे लेकिन बाड़ में स्वतंत्र राजनेतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए|
- इस वंश के 37वें राजा अजयपाल ने सभी गढ़पतियों को जीतकर गढ़वाल भूमि का एकीकरण किया। इसने अपनी राजधानी चांदपुर गढ को पहले देवलगढ़ फिर 1517 ई. में श्रीनगर में स्थापित किया।
- परमार शासकों को लोदी वंश के शासक बहलोद लोदी ने शाह की उपाधि से नवाजा , सर्वप्रथम बलभद्र शाह ने अपने नाम के आगे शाह जोड़ा|
- 1636 ई. में मुग़ल सेनापति नवाजतखां ने दून-घाटी पर हमला कर दिया ओर उस समय की गढ़वाल राज्य की संरक्षित महारानी कर्णावती ने अपनी वीरता से मुग़ल सैनिको को पकडवाकर उनके नाक कटवा दिए , इसी घटना के बाद महारानी कर्णावती को “नाककटी रानी” के नाम से प्रसिद्ध हो गयी।
- परमार राजा प्रथ्विपति शाह ने मुग़ल शहजादा दाराशिकोह के पुत्र शुलेमान शिकोह को आश्रय दिया था इस बात से औरेंजेब नाराज हो गया था|
- 1790 ई. में कुमाऊॅ के चन्दो को पराजित कर, 1791 ई. में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया लेकिन पराजित हो गए। गढ़वाल के राजा ने गोरखाओं से संधि के तहत 25000 रूपये का वार्षिक कर लगाया और वचन लिया की ये पुन: गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे , लेकिन 1803 ई. में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गौरखाओ ने भूकम से ग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर उनके काफी भाग पर कब्ज़ा कर लिया।
- 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओ से हुए युद्ध में प्रधुमन्न शाह की मौत हो गई , इस प्रकार सम्पूर्ण गढ़वाल और कुमाऊॅ में नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया।
- प्रधुमन्न शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतमशाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, जबकि दुसरे पुत्र सुदर्शनशाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे और उनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल लार्ड हेस्टिंग्ज ने अक्तूबर 1814 में गोरखा के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजी और 1815 को गढ़वाल को स्वतंत्र कराया , लेकिन अंग्रेजों को लड़ाई का खर्च न दे सकने के कारण गढ़वाल नरेश को समझौते में अपना राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा।
- शुदर्शन शाह ने 28 दिसम्बर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी गढ़वाल स्थापित की। टिहरी राज्य पर राज करते रहे तथा भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को 1 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया।
- पंवार शासको के काल में अनेक काव्य रचे गए जिनमे सबसे प्राचीन मनोदय काव्य है जिसकी रचना भरत कवि ने की थी|
आधुनिक काल (Modern Period)
उत्तराखंड के आधुनिक काल के इतिहास में हम गोरखा शासन तथा ब्रिटिश शासन के बारे में अध्ययन करेंगे|
गोरखा शासन
- गोरखा नेपाल के थे , गोरखाओ ने चन्द राजा को पराजित कर 1790 में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया|
- कुमाऊॅ पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया लेकिन पराजित हो गये और फरवरी 1803 को संधि के विरुद्ध जाकर गोरखाओं ने अमरसिंह थापा और हस्तीदल चौतारिया के नेतृत्व में पुन: गढ़वाल पर आक्रमण किया और सफल हुए।
- 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रधुम्न्ना शाह और गोरखों के बीच देहरादून के खुडबुडा मैदान में युद्ध हुआ और गढ़वाल नरेश शहीद हो गए|
- 1814 ई. में गढ़वाल में अंग्रेजो के साथ युद्ध में पराजित हो कर गढ़वाल राज मुक्त हो गया, अब केवल कुमाऊॅ में गोरखाओं का शासन रह गया|
- कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्डनर ने अप्रैल 1815 में कुमाऊॅ के अल्मोड़ा को व जनरल ऑक्टरलोनी ने 15, मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मालॉव का किला जीत लिया।
- 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर तथा गोरखा शासक बमशाह के बीच हुई संधि के तहत कुमाऊॅ की सत्ता अंग्रेजो को सौपी दी गई।
- कुमाऊॅ व गढ़वाल में गोरखाओं का शासन काल क्रमश: 25 और 10.5 वर्षों तक रहा।जो बहुत ही अत्याचार पूर्ण था इस अत्चयारी शासन को गोरख्याली कहा जाता है|
ब्रिटिश शासन
- अप्रैल 1815 तक कुमाऊॅ पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजो ने टिहरी को छोड़ कर अन्य सभी क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रान्त का भाग बना दिया, और इस क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर को नियुक्त किया।
- कुछ समय बाड़ कुमाऊँ जनपद का गठन किया गया और देहरादून को 1817 में सहारनपुर जनपद में सामिल किया गया|
- 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल के मुख्यालय को श्रीनगर से हटाकर पौढ़ी लाया गया व पौढ़ी गढ़वाल नामक नये जनपद का गठन किया।
- 1854 में कुमाऊँ मंडल का मुख्यालय नैनीताल बनाया गया
- 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक दो जिलो में बाँट दिया गया, और स्वतंत्रता तक कुमाऊॅ में केवल 3 ही ज़िले थे (अल्मोड़ा, नैनीताल, पौढ़ी गढ़वाल) और टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में थी
- 1891 में उत्तराखंड से नॉन रेगुलेशन प्रान्त सिस्टम को समाप्त कर दिया गया|
- 1902 में सयुंक्त प्रान्त आगरा एवं अवध का गठन हुआ और उत्तराखंड को इसमें सामिल कर दिया गया|
- 1904 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को हिल स्टेट का नाम दिया गया|
स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखंड की भूमिका (The Role of Uttarakhand in the Independence Movement)
1857 की क्रांति
- 1857 में चम्पावत जिले के बिसुंग गाँव के कालू सिंह महरा ने कुमाऊॅ क्षेत्र में क्रांतिवीर संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन चलाया। उन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव भी प्राप्त है|
- कुमाऊॅ क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितम्बर 1857 को एक हजार से अधिक क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया|
1857 के बाद आन्दोलन
- 1870 ई. में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की और 1871 से अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई|अल्मोड़ा अकबार 1918में बंद हो गया इसके बाड़ 1918 से बद्रीदत्त पाण्डेय ने शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया|
- 1886 में ज्वालादत्त जोशी ने कांग्रेस के कलकत्ता में आयोजित सम्मलेन में भाग लिया|
- पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने 1903 में हैप्पी क्लब नाम की एक संस्था बनायीं |
- 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गयी|
- तिलक और बेसेंट द्वारा 1914 चलाये गए होम रूल लीग आन्दोलन से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पाण्डेय , चिरंजीलाल और हेमचंद ने उत्तराखंड में होमरुल लीग आन्दोलन चलाया|
- 1916 में गोविन्द बल्लभ पन्त, हरगोविंद पन्त , बद्रीदत्त पाण्डेय आदि नेताओ के प्रयास से कुमाऊं परिषद का गठन हुआ, 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया|
- बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसूया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, इन दोनों नेताओ ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया|
- 1920 में गांधीजी द्वारा शुरू किए गये असहयोग आन्दोलन में कई लोगो ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया और कुमाऊ मण्डल के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर कुली-बेगार न करने की शपथ ली और इससे संबंधीत रजिस्ट्री को नदी में बहा दिया गया|
- 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल रायफल के सैनिक वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलने से इंकार कर दिया था, यह घटना ‘पेशावर कांड’ के नाम से प्रसिद्ध है।, पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरु ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मानाने की घोषणा की|
भारत छोड़ो आन्दोलन में उत्तराखंड की भूमिका
- अल्मोड़ा के धामगो में 25 अगस्त 1942 को सेना व जनता के बीच पत्थर व गोलियों का युद्ध हुआ|
- अल्मोड़ा के सल्ट में 5 सितम्बर 1942 खुमाड़ नामक स्थान पर सेना ने जनता पर गोलिया चला दी इसमें कई लोग शहीद हुए , इस घटना के कारण महात्मा गाँधी ने सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा , सल्ट के खुमाड़ में प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को शहीद दिवस मनाया जाता है|
स्वंत्रता आन्दोलन में उत्तराखंड की महिलाओ की भूमिका
- उत्तराखंड से स्वंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाये कुंती वर्मा , पद्मा जोशी , दुर्गावती पन्त ,जानकी देवी ,शकुंतला देवी , भिवेडी देवी, बिशनी देवी शाह आदि थी
स्वंत्रता आन्दोलन के दौरान उत्तराखंड में प्रकाशित प्रमुका पत्र- पत्रिकाएं
- अल्मोड़ा अकबार- अल्मोड़ा अकबार 1871 में अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ.
- शक्ति – 1918 में अल्मोड़ा अकबार के बंद हो जाने के बाद बद्रीदत्त पाण्डेय ने शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया.
- गढ़वाली – पं गिरिजादत्त नैथानी के सम्पादकत्व में 1905 में देहरादून से प्रकाशित.
- कर्मभूमि- 1939 में भक्तदर्शन और भैरवदत्त के सम्पादकत्व में लेंसडाउन से प्रकाशित.
- युगवाणी- 1941 में देहरादून से प्रकाशित.
उत्तराखंड में हुए प्रमुख जन-आन्दोलन
कुली बेगार आन्दोलन
- अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजो के सामान को एक गाँव से दुसरे गाँव तक गाँव वालो को ढोना पड़ता था तथा इसका लेखा जोखा गाँव के मुखिया के पास रजिस्टर में रहता था,जिसे बेगार रजिस्टर कहा जाता था|
- 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पाण्डेय , हरगोविंद पन्त व चिरंजीलाल के नेतृत्व में लगभग 40 हजार आंदोलनकारियो ने बेगार नहीं देने का संकल्प लिया और कुली बेगार से सम्बंधित सभी रजिस्टर जला दिए और यही से इस कुप्रथा का अंत हो गया|
टिहरी राज्य आन्दोलन
- टिहरी में प्रजातान्त्रिक शासन की मांग को लेकर 20 वी शताब्दी के तीसरे दशक से ही कई जनांदोलन होने लगे थे टिहरी में 1939 में श्री देवसुमन, दौलतराम, नागेन्द्र सकलानी आदि के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई और आन्दोलन का विस्तार हुआ, मई 1944 में श्री देवसुमन अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर बैठ गये और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई |
- 1948 में कीर्तिनगर आन्दोलन हुआ जिसमे भोलूराम और नागेन्द्र शहीद हुए|
- राजा मानवेन्द्र शाह ने 1949 में विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 1 अगस्त 1949 से टिहरी संयुक्त उत्तरप्रदेश का जिला बन गया।
डोला पालकी अन्दोलान
- इस आन्दोलन से पूर्व राज्य के शिल्पकारो को शादी विवाह के अवसर पर डोला पालकी में बैठेने का अधिकार नहीं था|
- जयानंद भारती द्वारा 1930 के आसपास डोला पालकी आन्दोलान चलाया गया जिसके बाद शिल्पकारो को यह अधिकार मिल गया|
कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आन्दोलन
- यह अन्दोलन भ्रष्टाचार के खिलाप था जो अल्मोड़ा के बडियार रेत (लमगड़ा) गाँव से शुरू हुआ|
कोटा खर्रा आन्दोलन
- इस आन्दोलन का उद्देश्य राज्य के तराई वाले क्षेत्रो में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों को भूमि वितरण करना था|
पृथक राज्य निर्माण के लिए आन्दोलन (Movement for separate state creation)
- उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम 5-6 मई 1938 को श्रीनगर (गढ़वाल) में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेसन में उठाई गयी.
- श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य के निर्माण हेतु 1938 में दिल्ली में गढ़देश सेवा संघ नाम का संगठन बनाया, जिसका नाम बाद में हिमालय सेवा संघ कर दिया गया.
- 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन बनाया गया जिसका उद्देश्य उत्तराखंड और हिमांचल प्रदेश को मिलकर एक हिमालयी राज्य बनाना था.
- 24 व 25 जून 1967 को रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया.
- 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया.
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पी. सी. जोशी ने 3 अक्टूबर 1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया.
- 1969 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया, और इस परिषद के सदस्यों ने 1972 में दिल्ली के वोट क्लब पर धरना दिया.
- 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया.
- 1979 में त्रेपन सिंह नेगी द्वारा उत्तराचल राज्य परिषद का गठन किया गया.
- 25 जुलाई 1979 में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया तथा इसका पहला अध्यक्ष कुमाऊं विश्विद्यालय के कुलपति डॉ. देवीदत्त पन्त को बनाया गया.
- उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर 1984 में आल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने 900 किमी की साइकिल यात्रा निकाली.
- उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर 23 अप्रैल 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल के नेता त्रिवेन्द्र पंवार ने संसद में एक पत्र बम फेंका.
- 1988 में शोबन सिंह जीना द्वारा ‘उत्तराँचल उत्थान परिषद‘ का गठन किया गया.
- 1989 में ‘उत्तराँचल संयुक्त संघर्ष समिति‘ का गठन किया गया.
- उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य निर्माण का पहला प्रस्ताव 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट द्वारा रखा गया.
- 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने एक दस्तावेज जारी कर गैरसैण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया , इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लू प्रिंट माना जाता है.
- उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जनवरी 1993 में रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक समिति ( कौसिक समिति ) का गठन उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए किया.
- 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण करने की घोसणा की.
- उत्तरप्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 27 जुलाई 2000 को लोक सभा में पेश किया गया , यह विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा तथा 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के. आर. नारायण ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी .
- 9 नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलो को अलग कर देश के 27 वे तथा हिमालयी राज्यों में 11 वे राज्य के रूप में उत्तराँचल राज्य का गठन किया गया, तथा 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया.
FAQs on History of Uttarakhand in Hindi
उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ?
9 नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलो को अलग उत्तराँचल राज्य का गठन किया गया, तथा 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया।
उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है?
देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है, जबकि गैरसैण (भराड़ीसैंण) राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है।
उत्तराखंड के पहले शासक कौन थे?
उत्तराखंड के पहले शासक कुणिन्द वंश के थे, जो मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। बाद में इस क्षेत्र में विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों का शासन रहा।
उत्तराखंड के इतिहास में ‘गढ़वाल’ और ‘कुमाऊं’ का क्या महत्व है?
गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड के दो प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। गढ़वाल का ऐतिहासिक संबंध पौराणिक कथाओं, प्राचीन मंदिरों और शाही वंशों से है, जबकि कुमाऊं क्षेत्र का संबंध विभिन्न ऐतिहासिक राजवंशों और संघर्षों से जुड़ा हुआ है। इन दोनों क्षेत्रों का इतिहास राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उत्तराखंड में कौन-कौन से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं?
उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं।
Beautiful……..